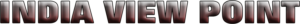सवर्ण बनाम गैर-सवर्ण की लड़ाई नहीं, बल्कि असमानता के ख़िलाफ़ संघर्ष
हरिगोविंद विश्वकर्मा
कभी-कभी लगता है कि भारत में सूचना सत्यापन की प्रवृत्ति अत्यंत कमज़ोर है। यहां लोगों में सूचना को वेरिफाई करने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया पर बिना जाँच किए केवल अपने रुचिकर कंटेंट को साझा करना खतरनाक प्रवृत्ति बन गई है। यही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) नई नियमावली के साथ हो रहा है। UGC ने पिछले महीने “प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन्स रेगुलेशन्स, 2026” जारी किया जो 2013 की नियमावली का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य महिलाओं, दिव्यांगों, SC, ST और OBC समुदायों के छात्रों, अध्यापकों और अन्य स्टाफ़ के साथ किसी भी जातिगत या लैंगिक भेदभाव और शोषण को रोकना तथा शिक्षण संस्थानों में समावेशी और समान अवसर वाला वातावरण सुनिश्चित करना है।। अब सवर्ण समाज के ही कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी सोशल मीडिया ज्ञान का हवाला देकर इसे सवर्ण समाज के पुरुषों के ख़िलाफ़ बताते हुए इसे ‘काला क़ानून’ कह रहे हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है- ‘हम, भारत के लोग… शिक्षा, रोज़गार और उन्नति के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए… राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के दृढ़ संकल्प के साथ, अपनी इस संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।’ इसे अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया। लेकिन कई सदियों से अपने को सुपीरियर मानने वाला और गैरसवर्णों के शोषण को न्यायोचित ठहराने वाला सवर्ण समाज क्या मन से संविधान को स्वीकार सका है? निष्कर्ष सरल है, ऐसा मनोवैज्ञानिक स्वीकृति नहीं मिली।
पिछले 75-76 साल में इस देश संविधान में सबको जाति, धर्म, लिंग, भाषा या आर्थिक हैसियत से परे बराबरी का दर्जा देने के प्रावधान पर कितना अमल कर पाया। ज़ाहिर सी बात है कि न देश संविधान के आदर्शों के अनुसार चल सका, और न ही सवर्ण समाज में न्यायिक विवेक विकसित हो सका। यह वजह है कि कभी सुनते हैं कि सवर्ण छात्रों, अध्यापकों और अन्य स्टाफ के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से कभी रोहित वेमुला जैसे छात्रों ने संस्थान में पक्षपात और भेदभाव से पीड़ित होकर आत्महत्या की, तो कभी आदिवासी डॉ. पायल तड़वी को इसी कारण से क्षुब्ध होकर जीवन समाप्त करना पड़ा।” ऐसे घटनाक्रम यह दर्शाते हैं कि आज भी सामाजिक और संस्थागत भेदभाव से पीड़ित लोगों पर अत्याचार का दवाब मौजूद है। यह फेहरिस्त साबित करती है कि 21वीं सदी में भी सवर्ण वर्ग के कुछ लोगों में पूर्वाग्रह और भेदभाव की मानसिकता कायम है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है।
ऐसे परिवेश में UGC नियमावली की पृष्ठभूमि में यह बताना बहुत ज़रूरी है कि देश में किस समाज की आबादी कितनी है और संस्थानों में प्रतिनिधित्व कितना है। वैसे तो यहां आख़िरी बार जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद कांग्रेस के सवर्ण नेताओं ने जातीय जनगणना नहीं होने दी। स्वतंत्रता आंदोलन में सवर्णों का ही वर्चस्व था, तो आज़ाद भारत में मलाई उन्होंने ही काटी और अब तक काट रहे हैं। इससे सत्ता और संसाधनों पर उनका ही वर्चस्व स्थापित हो गया। जातीय जनगणना के अभाव में जाति-आधारित आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। फिर भी विभिन्न अध्ययनों और अनुमानों के अनुसार, 140 करोड़ आबादी वाले देश में सवर्ण केवल 12 से 14 प्रतिशत यानी 15 से 18 करोड़ हैं। दलित और OBC की आबादी तक़रीबन 70 फ़ीसदी यानी तक़रीबन 100 करोड़ है। देश में इस समय कुल 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इनमें केवल 1 SC, 1 ST और 4 OBC वाइस चांसलर हैं। शेष 38 VC सवर्ण हैं। इन संस्थानों में 80.8 फ़ीसदी प्रोफेसर सवर्ण हैं, जबकि SC, ST और OBC समुदायों से आने वाले प्रोफेसरों का अनुपात क्रमशः 6.8, 1.5 और 4.1 फ़ीसदी ही है।
अल्पसंख्यक होने के बावजूद देश की सत्ता और संस्थानों पर सवर्णों का असमान वर्चस्व है। UGC के मौजूदा नियमों में वास्तविक लाभार्थी वही वर्ग है। घाटे में तो गैर-सवर्ण हैं। मज़े की बात है कि सवर्ण ही इसे काला क़ानून बता रहे हैं। दरअसल, मौजूदा परिवेश में विडंबना यह है कि नई UGC नियमावली उन्हीं के पक्ष को कमज़ोर कर देती है, जिनके साथ भेदभाव और शोषण रोकने के लिए इसे बनाया गया है। यानी मौजूदा स्वरूप में नया नियम जातिगत भेदभाव और शोषण के शिकार लोगों को इंसाफ़ दिला ही नहीं सकता, क्योंकि जातिगत या लैंगिक भेदभाव या शोषण की प्रारंभिक जांच करने वाली संस्थान की 10-सदस्यीय कमेटी की संरचना ही समस्या को उजागर करती है। इसमें सात सदस्य सवर्ण होंगे। यानी न्याय करने वाली कमेटी में सवर्ण बहुमत में रहेगे। कमेटी में SC-ST और OBC के 1-1 सदस्य यानी कुल 3 ही प्रतिनिधि होंगे। इसका अध्यक्ष VC या Principal होगा। स्वाभाविक तौर पर सवर्ण ही होगा। शेष छह में 1-1 सदस्य महिला और दिव्यांग होंगे। ज़्यादा संभावना है, वे भी सवर्ण सदस्य होंगे। समिति में शेष 4 पदों में से 2 प्रोफेसर और 2 समाज के प्रबुद्ध और सम्मानित वर्ग के सदस्य होंगे। सीधी सी बात है, इस संरचना में भी सवर्ण वर्चस्व बना ही रहेगा।
सवर्ण अध्यक्ष और सवर्ण सदस्यों की बहुमत वाली कमेटी शिकायत को ही फ़र्ज़ी करार देकर गैर-सवर्ण शिकायतकर्ता को ही दंडित कर सकती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सवर्ण ऐसा क्यों करेंगे। अरे भाई, ऐसा अब तक करते आए हैं। शोषण को ये लोग अपना विशेषाधिकार मानते हैं। क्योंकि शोषण करने की मानसिकता पीढ़ी-दर-पीढ़ी सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बन गई है। वस्तुतः देश के सवर्णों में विशेषकर उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आधुनिक और AI के दौर में भी ‘जीयो और जीने दो की’ मानवीय व न्यायिक प्रवृत्ति और न्यायिक विवेक पनप ही नहीं पाया है। कथित तौर पर केवल ख़ुद को ही प्रतिभाशाली मानने वाला यह वर्ग गैर-सवर्णों से गहरी सामाजिक शत्रुता रखता है। यह हालत इसलिए भी है, क्योंकि आबादी में अल्पसंख्यक यानी 14 फ़ीसदी होने के बावजूद देश के 90 फ़ीसदी संसाधनों, नौकरियों, कारोबारों और संपत्तियों पर इसी सवर्ण समाज का क़ब्ज़ा है।
सदी-दर-सदी वर्चस्व में रही सवर्ण सामाजिक संरचना बहुमत में अब इतनी स्वार्थपरक हो गई हैं कि इस समाज के लोग केवल अनुमानित फ़र्ज़ी मुक़दमे का हव्वा खड़ा करके UGC की नियमावली को काला कानून बता रहे हैं। यह सर्वविदित है कि देश के हर क़ानून का 1-2 फ़ीसदी दुरुपयोग होता है। यहां तक कि कभी-कभी बलात्कार-विरोधी क़ानून का भी दुरुपयोग हो जाता है। तो क्या इस क़ानून को भी इसी तर्क से ख़त्म कर दिया जाए? UGC को लेकर सवर्णों की संभावित दुरुपयोग की लॉजिक मानने का मतलब सारे क़ानून ही ख़त्म कर दिए जाएं। यानी रेप क़ानून ख़त्म करके बलात्कारियों को रेप करने के लिए खुला छोड़ दिया जाए। अब सवाल यह है कि क्या सवर्ण लोग इस देश को क़ानूनविहीन अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं? यानी इसे जंगल राज में तब्दील करना चाहते हैं? जहाँ केवल इसलिए क़ानून न हों, क्योंकि उनके दुरुपयोग की आशंका जताई जाती है?
वस्तुतः किसी भी क़ानून का दुरुपयोग उसी स्थिति में माना जाता है, जब उसका शिकार कोई निर्दोष व्यक्ति हो जाए। यानी जिसने अपराध किया ही न हो या जिसका अपराध से कोई सरोकार ही न हो, उसके ख़िलाफ़ अगर किसी क़ानून विशेष का प्रयोग हो जाए तो वह दुरुपयोग है। लेकिन इस तरह के दुरुपयोग सांख्यिकीय रूप से अत्यंत दुर्लभ हैं, यानी सौ केसों में एकाध। उदाहरण के तौर पर, पिछले कई वर्षों से लोगों के निशाने पर एससी-एसटी एक्ट और दहेज-विरोधी कानून रहते हैं। इन दोनों क़ानूनों के दुरुपयोग का अनुपात भी सौ केस में एकाध केस होता है। अगर सौ में एकाध केस ऐसा है, जहां क़ानून का दुरुपयोग हुआ है तो इससे यह निष्कर्ष निकालना कि क़ानून ही ग़लत है, पूरी तरह अनुचित है। क्या वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति पर एससी-एसटी एक्ट लगाया गया है, जिसका विवाद से दूर-दूर तक कोई संबंध ही न रहा हो? ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं।
सीधी सी बात है, किसी भी क़ानून के दायरे में वही व्यक्ति आता है, जब या तो वह उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा हो। जो लोग महिलाओं, दिव्यांगों, SC-ST और OBC समुदायों से जुड़े छात्रों, अध्यापकों और अन्य स्टाफ़ के साथ किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव या शोषण करेंगे ही नहीं, उनके ख़िलाफ़ इस क़ानून के दुरुपयोग का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा थोड़ी ही होगा कि जो लोग शांतिपूर्ण ढंग से काम करते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी इस क़ानून के तहत कार्रवाई हो जाएगी। हर क़ानून अपराध करने वालों को दंडित करता है। तो फिर इस क़ानून को ‘सवर्ण-विरोधी’ कहने का आधार आख़िर है क्या?
दरअसल, इस देश का संविधान बनाया गया और शासन के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था चुनी गई। इसके पीछे मंशा यही थी कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा और क्षेत्र से पहले हर नागरिक का सर्वांगीण विकास हो। संविधान की मूल भावना यही थी कि विकास किसी एक वर्ग तक सीमित न रहे, बल्कि दलितों और पिछड़े वर्ग का भी विकास हो। महिलाओं का विकास हो। संतुलित विकास तो तभी संभव है, जब गैर-सवर्णों और महिलाओं को भी सरकार में प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन आज़ादी के बाद सत्ता में आई कांग्रेस के नेतृत्व में सवर्णों का वर्चस्व स्थापित हो गया। विधायिका (सांसद और विधायक), कार्यपालिका (नौकरशाही) और न्यायपालिका (जज) यानी लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में निर्णायक पदों पर सवर्णों की प्रधानता स्थापित हो गई। कहने भर के लिए भर्ती के लिए परीक्षाएं होती थीं, लेकिन निर्णायक मंडलों में अक्सर सवर्णों का बहुमत होता रहा। ये लोग सवर्ण छात्रों का चयन ज़्यादा करते हैं। इसीलिए देश की नौकरशाही में सवर्णों की अत्यधिक उपस्थिति बनी हुई है।
अगर मीडिया को चौथा स्तंभ मान लें तो उसमें भी सवर्ण का वर्चस्व है, क्योंकि विभिन्न अध्ययनों में यह सामने आया है कि मीडिया संस्थानों में लगभग 90–95 फ़ीसदी हिस्सेदारी सवर्णों की है। व्यवहार में देखें तो अधिकांश लेखन पर सवर्ण पत्रकारों का वर्चस्व दिखाई देता है। ख़ुद को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी समझने वाले ये सारे सवर्ण पत्रकार आरक्षण को प्रतिभा-विरोधी मानते हैं। इनका प्रतिभा-बोध अक्सर सामाजिक पहचान, विशेषकर सरनेम, से तय होता दिखाई देता है। जबकि यह सच है कि आपकी सफलता में अगर आपके सरनेम का ज़्यादा योगदान है, तो इसका मतलब आप सच में प्रतिभाशाली नहीं हैं। आपके पास कितना भी ज्ञान और अनुभव हो, लेकिन प्रतिभा का पर्याय बन चुका सरनेम नहीं है, तो मीडिया में आगे बढ़ने के अवसर बेहद सीमित हो जाते हैं। नौकरी कभी-कभार अपवाद स्वरूप मिल भी गई तो कम से कम सरनेम के अभाव में संपादक नहीं बन सकते। संपादक तो सवर्ण ही बनेंगे। ज़मीन पहले से ही सवर्णों के पास थी, आज़ाद भारत में नौकरी पर भी उन्हीं का क़ब्ज़ा हो गया। और मीडिया यानी सूचना पर क़ब्ज़ा, तो गैर-सवर्णों के हिस्से में सत्ता, संसाधन और अभिव्यक्ति, तीनों में क्या बचता है?
मान लीजिए दो बच्चे हैं। एक बच्चे के पास बिजली, रोशनी और पढ़ने का माहौल है। उसे गाइड करने के लिए ट्यूटर के रूप में एक टीचर रखा गया है। दूसरे बच्चे के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन परीक्षा और मूल्यांकन की कसौटी दोनों के लिए एक समान रखी गई है। ऐसे में ज़ाहिर है, सुविधा संपन्न बच्चे के अंक अधिक आएंगे, इसका मतलब यह थोड़ी है कि दूसरे बच्चे में प्रतिभा नहीं है। आपको प्रतिभा का आकलन करना है तो पहले दोनों की सुविधाएं समान करनी की चाहिए। प्रतिभा वह प्राकृतिक या अर्जित क्षमता है, जो निरंतर अभ्यास, सीखने और अनुभव से विकसित होकर व्यक्ति को सामान्य से बेहतर प्रदर्शन करने योग्य बनाती है। प्रतिभा व्यक्ति की रुचि, लगन और मेहनत के साथ मिलकर उसे दूसरों से अलग पहचान दिलाती है। प्रतिभा व्यक्ति की अपनी क्षमता, रुचि, मेहनत और अभ्यास से जुड़ी होती है, न कि उसके नाम, जाति या परिवार के सरनेम से। यानी सरनेम कभी भी प्रतिभा का प्रमाण नहीं हो सकता। कहने का मतलब दो योद्धाओं में कौन श्रेष्ठ है, इसका सही फ़ैसला तभी हो पाएगा न, जब युद्ध का मैदान, हथियार और परिस्थितियां दोनों के लिए एक जैसी हों।
भारत में ज़मीन का असमान वितरण किसी ऐतिहासिक दुर्घटना का नहीं, बल्कि यह सदियों पुरानी सामाजिक और राजनीतिक संरचना का परिणाम है। प्राचीन भारत में भूमि का स्वामित्व मुख्यतः प्रभुत्वशाली वर्णों, विशेषकर ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के पास केंद्रित था, जबकि शूद्र, अन्य पिछड़े वर्ग और आदिवासी खेती करते थे। ये लोग खेत का लगान यानी कर चुकाते थे, लेकिन क़ानूनी या सामाजिक रूप से भूमि के मालिक नहीं बन सकते थे। राजाओं द्वारा ब्राह्मणों को अग्रहार और ब्रह्मदेय के रूप में दी गई भूमि कर-मुक्त और स्थायी रहती थी, जिससे उनके पास लंबे समय तक संपत्ति जमा होती रही। सामंती व्यवस्था और ज़मींदारी प्रणाली ने इस असमानता को और गहरा दिया, क्योंकि सवर्ण वर्ग के ज़मींदारों को क़ानूनी मालिकाना हक़ मिला, जबकि गैर-सवर्ण किसान और मजदूर और इस व्यवस्था में वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी किरायेदार या भूमिहीन बने रहे।
ब्रिटिश शासन के दौरान स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement Act, 1793) और अन्य भूमि क़ानूनों ने इस पहले से मौजूद असमानता को क़ानूनी वैधता दे दी। स्वतंत्रता के बाद ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के प्रयास हुए, लेकिन कई कारणों से जैसे फर्जी बंटवारे, बेनामी हस्तांतरण और सामाजिक दबाव, भूमि का बड़ा हिस्सा व्यवहार में सवर्णों के पास ही बना रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि आज भी भारत में बड़े ज़मींदार और संपन्न किसान ज़्यादातर सवर्ण हैं, जबकि दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्ग भूमिहीन या अल्पभूमि-स्वामी हैं। यही ऐतिहासिक और संरचनात्मक असमानता आज़ादी के दशकों बाद भी जारी है। शोध बताते हैं कि दलित समुदाय में आधे से अधिक परिवार भूमिहीन हैं, जबकि सवर्णों में भूमिहीनता अत्यंत नगण्य है। यही असमानता आगे चलकर शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच को प्रभावित करती है। ज़मीन सिर्फ़ संपत्ति नहीं, बल्कि शक्ति और स्थिरता का स्रोत है और यही कारण है कि यह ऐतिहासिक रूप से कुछ समुदायों के पास ही केंद्रित रही है।
ऐसे में जब सरकार, राज्य या सरकारी संस्थान भेदभाव और असमानता को दूर करने के लिए कोई नियमावली या नीतियां लाती हैं, तो उसे “अनुचित हस्तक्षेप” की तरह देखा जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि ये प्रयास किसी के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि सदियों से चले आ रहे भेदभाव और असमानता को दूर करके समाज को संतुलित करने की कोशिश हैं। यह बहस योग्यता बनाम अयोग्यता की नहीं, बल्कि अवसरों की असमान उपलब्धता की है। सवाल यह है कि योग्यता को पनपने का अवसर सबको बराबर मिला है या नहीं। जब शुरुआती रेखा ही असमान हो, तो दौड़ को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। यह संघर्ष जातियों की आपसी टकराव का नहीं, बल्कि संसाधनों और अवसरों की असमान संरचना को पहचानने और सुधारने का है। जब तक इसे नहीं समझा जाएगा, तब तक हर सुधार ‘किसी के ख़िलाफ़’ ही लगता रहेगा। इसलिए इस विषय पर हर पक्ष को ईमानदारी से बिना पूर्वाग्रहित हुए सोचने की ज़रूरत है।